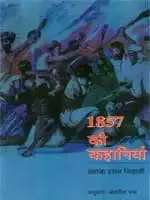|
कहानी संग्रह >> 1857 की कहानियाँ 1857 की कहानियाँख्वाजा हसन निजामी
|
251 पाठक हैं |
||||||
इन कहानियों की लोकप्रियता इतनी है कि उर्दू में ‘बेगमात के आंसू’ नाम से इसके 14 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
दिल्ली के शाही खानदान पर सन् 1857 के गदर में जो कुछ बीती, इस पुस्तक में
उनकी दुखभरी तथा दर्दनाक परिस्थियाँ इस प्रकार प्रस्तुत की गई हैं कि
आंसुओं को रोक पाना कठिन हो जाता है। इन कहानियों की लोकप्रियता इतनी है
कि उर्दू में ‘बेगमात के आंसू’ नाम से इसके 14
संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। स्व. शमसुल-उलेमा ख्वाजा हसन निजामी
(1880-1995) ने 500 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं जो भाषा तथा प्रस्तुतीकरण
की दृष्टि से उर्दू में विशेष महत्व रखती हैं। इनके छोटे-छोटे वाक्य,
दिल्ली की टकसाली भाषा में, दिल को छू जाते हैं और आँखों के सामने एक
तस्वीर-सी खींच देते हैं। इस पुस्तक के सम्पादक ख्वाजा अहमद फारुकी उर्दू के प्रसिद्ध अनुसंधात्सु तथा समालोचक हैं।
1857 की कहानियां
शम्सुल-उलेमा (प्रकांड विद्वान) ख्वाजा हसन
निज़ामी देहलवी
का जन्म सन् 1880 में हुआ था और देश की आजादी के बाद सन् 1955 में उनका
निधन हुआ। मैंने उनको अपने विद्यार्थी जीवन में और उनके निधन से कुछ महीने
पहले भी देखा था उनकी वेश-भूषा एक जैसी ही थी-गेरुआ लंबा कुर्ता, फकरीना
दुपट्टा-मशायख की टोपी,1 लम्बे लहराते बाल,आंखों में आकर्षण, बातचीत में
मोह लेने का प्रभाव और वाणी जैसे अमृत में घुली हुई।
ख्वाजा हसन निजा़मी ने पांच सौ से अधिक किताबें लिखी हैं जो भाषा और शैली में उर्दू में अद्वितीय हैं। दिल्ली की टकसाली भाषा में उनके छोटे-छोटे वाक्य दिल पर गहरा असर छोड़ते हैं और आँखों के सामने तस्वीर-सी खींच देते हैं। भाषा की इसी सादगी, सहजता और प्रवाह के कारण ही उनको ‘मुसव्विरे फितरत’’ (प्रकृति का चितेरा) कहा जाता है।
ख्वाजा हसन निजा़मी की शैली पर अब्दुल हलीम ‘शरर’ (1860-1926) और मुहम्मद हुसैन आजा़द (1830-1910) का गहरा प्रभाव है। उनके गद्य में मुहावरों का चटखारा है और वे अपनी भारतीय बुनियादों से अनभिज्ञ भी नहीं हैं। उसमें चुटकुलों-सा मजा है, चुटकियां और गुदगुदियां हैं लेकिन दर्द और संवेदना तो बेमिसाल है।
ख्वाजा हसन निजा़मी ने अपने सहपाठी और उत्पीड़ित शहजादों के संग उर्दू सीखी थी, जो गदर के बाद बड़ी संख्या में बस्ती हज़रत निजा़मुद्दीन और कूचा चेलान् दिल्ली में रहते थे। उनकी संगत में रहने से ख्वाजा हसन निजा़मी के दिल में शहजादों के प्रति हमदर्दी और स्नेह पैदा हुआ। उन्होंने इन उजड़े परिवारों से मिलकर उनके हालात पर कई किताबें लिखीं जो देश भर में बहुत लोकप्रिय हुईं। इनमें सबसे प्रसिद्ध पुस्तक ‘बेगमात के आंसू’ है, जिसने सन् 1857 की क्रान्ति की सच्ची कहानियां हैं और उन्हीं में से कुछ चुनी हुई कहानियां इस संग्रह में प्रस्तुत हैं।
मुल्ला वाहदी का कथन है कि एक बार ख्वाजा हसन निजा़मी सख्त बीमार हो गए। उनकी माता ने उन्हें एक दरवेश के बार भेजा तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुरशाह जफ़र के निकट संबंधी थे। उन बुजुर्ग ने इनके गले में नादे अली का तावीज डलवा दिया। माताजी गर्व से बोलीं, ‘‘मेरे बच्चे के लिए हिंदोस्तान के बादशाह ने नादे अली का नक्श दिया है।’’ ‘‘बादशाह’’ शब्द पर माता के आंसू निकल आये। ख्वाजा साहिब ने पूछा, ‘‘अम्मा, आप रोती क्यों हैं ?’’ उन्होंने उत्तर दिया, ‘‘बेटा अब वे बादशाह नहीं हैं। अंग्रेजों ने तख्त-ताज सब छीन लिए हैं।’’
(1) भारत के सूफी संतों द्वारा ओढ़ी जाने वाली एक विशेष प्रकार की टोपी।
ख्वाजा साहिब कहते हैं कि इस घटना ने उनके मन में शहजादों के प्रति हमदर्दी का ऐसा बीज बोया कि जब सन् 1922 में मदीना-ए-मुनव्वरा गए तो उस वक्त भी उन्होंने उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना की औऱ कहा, ‘‘ए दो जहान के सरदार, मैं दिल्ली के बरबाद शाहजादों का नाता-ओ-बुका (चीख-पुकार) पेश करता हूं। वे तख्त-ताज के लिए नहीं रोते। उन्हें रूखी रोटी का टुकड़ा और तन ढाँपने के लिए मोटा कपड़ा दरकार है। उनके अपमान और निरादर की हद हो चुकी है। अब खता पोश परवर्दिगार (गलतियों को छिपाने वाला पालनहार) से उन्हें माफी दिलवा दीजिए।
सन् 1911 ही में दिल्ली दरबार हुआ। उसमें एक प्रोग्राम आलिमों और पंडितों के सलाम का भी था। सम्राट जार्ज पंचम अपनी महारानी के साथ लालकिले के झरोखे में बैठ गए और किले की दीवार के नीचे और हिन्दू मुसलमान धार्मिक नेताओं ने एक साथ इकट्ठे होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। ख्वाजा हसन निजा़मी को भी बुलाया गया। वे घेर पर लिहाफ ओढ़े लेटे रहे और उस समारोह में शामिल नहीं हुए। कहते थे, ‘‘मुझसे यह देखा नहीं जाएगा कि जहां शाहजहां और उनकी औलाद ने दर्शन दिए हों वहां जार्ज पंचम विराजमान हों। फिर लिहाफ का लुत्फ दरबारों से ज्यादा है।’
’ यह तो अंग्रेजों के जमाने की बात थी। आजादी के बाद लाल किले में पहला आम मुशायरा हुआ और पंडित कैफी से चलने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहलवा भेजा कि मुझसे किल-ए-मुअल्ला का यह अनादर नहीं देखा जाएगा।
ख्वाजा हसन निजा़मी की किताब ‘बेगमात के आंसू’ सबसे पहले ‘गपरे-दिल्ली के अफ़सानों’ के नाम से प्रकाशित हुई थी और कई बार जब्त हुई। इसके बाद इस पुस्तक के चौदह संस्करण निकल चुके हैं। इसके कुछ अंश रेडियो से प्रसारित भी हो चुके हैं।
सन् 1857 के विद्रोह में दिल्ली के शाही खानदान पर क्या गुजरी ? इस दुखभरी औऱ दर्दनाक कहानी को ख्वाजा हसन निजा़मी ने ऐसी संवेदनशील शैली में प्रस्तुत किया है कि पढ़ते-पढ़ते आँसुओं पर काबू पाना कठिन हो जाता है। गदर के बारे में इन चुनी हुई कहानियों का संग्रह अपने मौलिक नाम के साथ नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है कि स्वतंत्र भारत में यह पहले से भी ज्यादा दिलचस्पी के साथ पढ़ा जाएगा।
ख्वाजा हसन निजा़मी ने पांच सौ से अधिक किताबें लिखी हैं जो भाषा और शैली में उर्दू में अद्वितीय हैं। दिल्ली की टकसाली भाषा में उनके छोटे-छोटे वाक्य दिल पर गहरा असर छोड़ते हैं और आँखों के सामने तस्वीर-सी खींच देते हैं। भाषा की इसी सादगी, सहजता और प्रवाह के कारण ही उनको ‘मुसव्विरे फितरत’’ (प्रकृति का चितेरा) कहा जाता है।
ख्वाजा हसन निजा़मी की शैली पर अब्दुल हलीम ‘शरर’ (1860-1926) और मुहम्मद हुसैन आजा़द (1830-1910) का गहरा प्रभाव है। उनके गद्य में मुहावरों का चटखारा है और वे अपनी भारतीय बुनियादों से अनभिज्ञ भी नहीं हैं। उसमें चुटकुलों-सा मजा है, चुटकियां और गुदगुदियां हैं लेकिन दर्द और संवेदना तो बेमिसाल है।
ख्वाजा हसन निजा़मी ने अपने सहपाठी और उत्पीड़ित शहजादों के संग उर्दू सीखी थी, जो गदर के बाद बड़ी संख्या में बस्ती हज़रत निजा़मुद्दीन और कूचा चेलान् दिल्ली में रहते थे। उनकी संगत में रहने से ख्वाजा हसन निजा़मी के दिल में शहजादों के प्रति हमदर्दी और स्नेह पैदा हुआ। उन्होंने इन उजड़े परिवारों से मिलकर उनके हालात पर कई किताबें लिखीं जो देश भर में बहुत लोकप्रिय हुईं। इनमें सबसे प्रसिद्ध पुस्तक ‘बेगमात के आंसू’ है, जिसने सन् 1857 की क्रान्ति की सच्ची कहानियां हैं और उन्हीं में से कुछ चुनी हुई कहानियां इस संग्रह में प्रस्तुत हैं।
मुल्ला वाहदी का कथन है कि एक बार ख्वाजा हसन निजा़मी सख्त बीमार हो गए। उनकी माता ने उन्हें एक दरवेश के बार भेजा तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुरशाह जफ़र के निकट संबंधी थे। उन बुजुर्ग ने इनके गले में नादे अली का तावीज डलवा दिया। माताजी गर्व से बोलीं, ‘‘मेरे बच्चे के लिए हिंदोस्तान के बादशाह ने नादे अली का नक्श दिया है।’’ ‘‘बादशाह’’ शब्द पर माता के आंसू निकल आये। ख्वाजा साहिब ने पूछा, ‘‘अम्मा, आप रोती क्यों हैं ?’’ उन्होंने उत्तर दिया, ‘‘बेटा अब वे बादशाह नहीं हैं। अंग्रेजों ने तख्त-ताज सब छीन लिए हैं।’’
(1) भारत के सूफी संतों द्वारा ओढ़ी जाने वाली एक विशेष प्रकार की टोपी।
ख्वाजा साहिब कहते हैं कि इस घटना ने उनके मन में शहजादों के प्रति हमदर्दी का ऐसा बीज बोया कि जब सन् 1922 में मदीना-ए-मुनव्वरा गए तो उस वक्त भी उन्होंने उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना की औऱ कहा, ‘‘ए दो जहान के सरदार, मैं दिल्ली के बरबाद शाहजादों का नाता-ओ-बुका (चीख-पुकार) पेश करता हूं। वे तख्त-ताज के लिए नहीं रोते। उन्हें रूखी रोटी का टुकड़ा और तन ढाँपने के लिए मोटा कपड़ा दरकार है। उनके अपमान और निरादर की हद हो चुकी है। अब खता पोश परवर्दिगार (गलतियों को छिपाने वाला पालनहार) से उन्हें माफी दिलवा दीजिए।
सन् 1911 ही में दिल्ली दरबार हुआ। उसमें एक प्रोग्राम आलिमों और पंडितों के सलाम का भी था। सम्राट जार्ज पंचम अपनी महारानी के साथ लालकिले के झरोखे में बैठ गए और किले की दीवार के नीचे और हिन्दू मुसलमान धार्मिक नेताओं ने एक साथ इकट्ठे होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। ख्वाजा हसन निजा़मी को भी बुलाया गया। वे घेर पर लिहाफ ओढ़े लेटे रहे और उस समारोह में शामिल नहीं हुए। कहते थे, ‘‘मुझसे यह देखा नहीं जाएगा कि जहां शाहजहां और उनकी औलाद ने दर्शन दिए हों वहां जार्ज पंचम विराजमान हों। फिर लिहाफ का लुत्फ दरबारों से ज्यादा है।’
’ यह तो अंग्रेजों के जमाने की बात थी। आजादी के बाद लाल किले में पहला आम मुशायरा हुआ और पंडित कैफी से चलने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहलवा भेजा कि मुझसे किल-ए-मुअल्ला का यह अनादर नहीं देखा जाएगा।
ख्वाजा हसन निजा़मी की किताब ‘बेगमात के आंसू’ सबसे पहले ‘गपरे-दिल्ली के अफ़सानों’ के नाम से प्रकाशित हुई थी और कई बार जब्त हुई। इसके बाद इस पुस्तक के चौदह संस्करण निकल चुके हैं। इसके कुछ अंश रेडियो से प्रसारित भी हो चुके हैं।
सन् 1857 के विद्रोह में दिल्ली के शाही खानदान पर क्या गुजरी ? इस दुखभरी औऱ दर्दनाक कहानी को ख्वाजा हसन निजा़मी ने ऐसी संवेदनशील शैली में प्रस्तुत किया है कि पढ़ते-पढ़ते आँसुओं पर काबू पाना कठिन हो जाता है। गदर के बारे में इन चुनी हुई कहानियों का संग्रह अपने मौलिक नाम के साथ नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है कि स्वतंत्र भारत में यह पहले से भी ज्यादा दिलचस्पी के साथ पढ़ा जाएगा।
कुलसूम ज़मानी बेगम
यह एक बेचारी दरवेशनी की सच्ची विपदा है जो
जमाने की
गर्दिश से उन पर गुजरी। उसका नाम कुलसूम ज़मानी बेगम था। यह दिल्ली के
अंतिम मुगल सम्राट जफ़र बहादुर शाह की लाडिली बेटी थीं।
कुछ साल हुए निधन हो गया। मैंने कई बार शहजादी साहिबा से खुद उनकी जबानी उनके हालात सुने हैं क्योंकि उनको हमारे हुजूर निजा़मुद्दीन औलिया महबूबे अलाही (प्रभु के प्यारे) से खास अकीदत (श्रद्धा) थी। इसलिए अकसर हाजिर होती थीं और मुझे दर्दनाक बातें सुनने का मौका मिलता था। नीचे जितनी भी घटनाएँ दी गई हैं या उनकी साहिबजादी जी़नत ज़मानी बेगम ने, जो अब तक जिंदा हैं और पंडित के कूचे में रहती हैं। ये घटनाएं इस प्रकार हैं।
जिस समय मेरे बाबाजान की बादशाहत खत्म हुई और तख्त-ताज लुटने का वक्त नजदीक आया तो दिल्ली के लालकिला मों कोहराम मचा हुआ था। चारों तरफ हसरत बरसती थी। सफेद-सफेद संगमरमर के मकान काले स्याह नज़र आते थे। तीन वक्त से किसी ने कुछ खाया न था। मेरी गोद में डेढ़ साल की बच्ची जी़नत दूध के लिए बिलखती थी। फिक्र और परेशानी के मारे न मेरे दूध रहा था और न किसी अन्ना के। हम सब इसी उदासी में बैठे थे कि जिल्ले सुबहानी (मुगल दौर में राजा को इसी उपाधि से संबोधित किया जाता था) का खास ख्वाजा सरा हमको बुलाने आया। आधी रात का वक्त, सन्नाटे का आलम, गोलों की गरज से दिल सहम जाते थे, लेकिन हुक्मे सुल्तानी (राजादेश) मिलते ही हम हाजिरी के लिए रवाना हो गए। हुजूर मुसल्ले (नमाज पढ़ने की चटाई) पर तशरीफ रखते थे। तसबीह (जपमाला) हाथ में थी। जब मैं सामने पहुंची और झुककर तीन मुजरे (बंदगी) बजा लाई तो हुजूर ने बहुत प्यार से अपने पास बुलाया और फरमाने लगे, ‘‘कुलसूम, लो अब तुमको खुदा को सौंपा। किस्मत में हुआ तो देख लेंगे। तुम अपने खाविंद (पति) को लेकर फौरन कहीं चली जाओ। मैं भी जाता हूं। जी तो नहीं चाहता कि इस आखिरी वक्त में तुम बच्चों को आंखों से ओझल होने दूं पर क्या करूं साथ रखने में तुम्हारी बरबादी का डर है। अलग रहोगी तो शायद खुदा कोई बेहतरी का सामान पैदा कर दे।’’
इतना फरमाकर हुजूर ने दस्ते मुबारक (कर कमल) दुआ के लिए, जो कंपन रोग के कारण कांप रहे थे, ऊपर उठाए और देर तक ऊंची आवाज में बारगाहे इलाही (अल्लाह का घर) में अर्ज करते रहे :
‘‘खुदा का वंद यह बेवारिस बच्चे तेरे हवाले करता हूं। ये महलों के रहने वाले जंगल वीरानों में जाते हैं। दुनिया में इनका कोई मददगार नहीं रहा। तेमूर के नाम की इज्जत रखियो और इन बेकस औरतों की इज्जत बचाइयो। परवर्दिगार (पालने वाला खुदा) यही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सब हिंदू-मुसलमान मेरी औलाद हैं और आजकल सब पर मुसीबत छाई हुई है। मेरे एमाल (कर्म) की शामत से इनको बेइज्जत न कर और सबको परेशानी से निजात दे।’’
इसके बाद मेरे सिर पर हाथ रखा। जी़नत को प्यार किया और मेरे खाविंद मिर्जा़ ज्यायुद्दीन को कुछ जवाहरात देकर नूर महल साहिबा को हमराह कर दिया। जो हुजूर की बेगम थीं।
पिछली रात को हमारा काफिला किले से निकला। इसमें दो मर्द और तीन औरतें थीं। मर्दों में एक मेरे खाविंद मिर्जा़ ज्यायुद्दीन और दूसरे मिर्जा़ उम्र सुल्तान, बादशाह के बहनोई थे। औरतों में एक मैं, दूसरी नवाब नूर महल और तीसरी हाफिज सुल्तान, बादशाह की समधन थीं। जिस वक्त हम रथ में सवार होने लगे तो तड़के का वक्त था। सब तारे छिप गए थे लेकिन सुबह का तारा झिलमिला रहा था हमने अपने भरे पूरे-घर पर आखिरी नजर डाली तो दिल भर आया और आंसू उमड़ने लगे। नवाब नूर महल की आंखों में आंसू भरे हुए थे और सुबह के तारे का झिलमिलाना नूरमहल की आंखों में नजर आता था।
आखिर लाल से हमेशा के लिए जुदा होकर कोराली गाँव में पहुँचे और वहां अपने रथवान के मकान पर रुके। बाजरे की रोटी और छाछ खाने को मिली। उस वक्त भूख में ये चीजें बिरयानी से भी ज्यादा मजेदार मालूम हुईं। एक दिन तो अमन से गुजर गया। लेकिन दूसरे दिन आस-पास के जाट और गूजर इकट्ठे होकर कोराली को लूटने चढ़ आए। सैकड़ों औरतें भी उनके साथ थीं जो चुड़ैलों की तरह हम लोगों से चिमट गईं। तमाम जेवर और कपड़े इन लोगों ने उतार लिए। जिस वक्त ये सड़ी बसी औरतें अपने मोटे-मोटे, मैले-मैले हाथों से हमारे गले को नोचती थीं तो उनके लहगों से ऐसी बू आती थी कि दम घुटने लगता था।
इस लूट के बाद हमारे पास इतनी भी बाकी न रहा जिससे एक वक्त की रोटी जुट सके। हैरान थे कि देखिए अब और क्या पेश आएगा। जी़नत प्यास के मारे रो रही थी। सामने से एक जमींदार निकला। मैंने बेबस होकर आवाज दी, ‘‘भाई थोड़ा पानी इस बच्ची को ला दे।’’ जमींदार फौरन एक मिट्टी के बरतन में पानी लाया और बोला, ‘‘आज से तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई।’’ यह जमींदार कोराला का खाता-पीता आदमी था। इसका नाम बस्ती था। उसने अपनी बैलगाड़ी तैयार करके हम सब को सवार किया और कहा कि तुम जहां चाहो पहुंचा दूंगा। हमने कहा, ‘‘अजारा, जिला मेरठ में मीर फै़ज अली शाही हकीम रहते हैं। उनसे हमारे खानदान के बहुत अच्छे मरासम (संबंध) हैं। वहां ले चलो।’’ बस्ती हमें अजारा ले गया। मगर मीर फै़ज अली ने ऐसा बुरा बर्ताव किया जिसकी कोई हद नहीं। साफ कानों पर हाथ रख लिए कि तुम लोगों को ठहराकर अपना घरबार तबाह नहीं करना चाहता। (मीर फै़ज अली की औलाद ने यह किताब पढ़ी तो मुझसे कहा कि बेगम साहिबा का बयान ठीक नहीं। मीर फै़ज अली ने उन सबको ठहराया था और मदद दी थी।
वह वक्त बहुत मायूसी का था। एक तो यह डर कि पीछे से अंग्रेज फौज आती होगी। इस पर हमारी हालत इतनी खराब कि हर आदमी की निगाह फिरी हुई थी। वे लोग जो हमारी आंखों के इशारे पर चलते और हर वक्त देखते रहते थे कि हम जो हुक्म दें वह फौरन पूरा किया जाए वही आज हमारी सूरत नहीं देखना चाहते थे। शाबाश है बस्ती जमींदार को कि उसने मुंह बोली बहन का आखिर तक साथ निभाया। बेबस होकर अजारे से रवाना हुए और हैदराबाद की राह पकड़ी। औरतें बस्ती की गाड़ी में सवार थीं और मर्द पैदल चल रहे थे। तीसरे दिन एक नदी के किनारे पहुंचे जहां कोयल के नवाब की फौज डेरा डालकर पड़ी हुई थी। उन्होंने जब सुना कि हम शाही खानदान के आदमी हैं तो बहुत खातिर की और हाथी पर चढ़ाकर नदी के पार उतारा। अभी हम नदी के पार उतरे ही थे कि सामने से फौज आ गई और नवाब की फौज से लड़ाई होने लगी।
मेरे खाविंद मिर्जा़ उम्र सुल्तान ने चाहा कि नवाब की फौज में शामिल होकर लड़ें मगर रिसालदार ने कहला भेजा कि आप औरतों को लेकर जल्दी चले जाएं।
हम जैसा मौका होगा देख लेंगे। सामने खेत थे जिनमें पकी हुई तैयार फसल खड़ी थी। हम लोग उसके अंदर छिप गए। जालिमों ने पता नहीं देख लिया था या अचानक ही गोली लगी। जो कुछ भी एक गोली खेत में आई जिससे आग भड़क उठी औऱ सारा खेत जलने लगा। हम सब वहां से निकलकर भागे पर हाय, कैसी मुसीबत थी—हमको भागना भी नहीं आता था। घास में उलझ-उलझ कर गिरते थे। सिर की चादरें वहीं रह गईं। नंगे सिर होश उड़े हुए हजार दिक्कत से खेत से बाहर आए। मेरे और नवाब महल के पांव लहूलुहान हो गए। प्यास के मारे जबानें बाहर निकल आईं। जी़नत को गश (मूर्छा) पर गश आ रहे थे। मर्द हमको संभालते थे लेकिन हमारा संभलना मुश्किल था।
नवाब नूर महल तो खेत से निकलते ही चकरा कर गिर पड़ीं और बेहोश हो गईं। मैं जी़नत को छाती से लगाए अपने खाविंद का मुंह देख रही थी और दिल में कहती थी कि अल्लाह हम कहां जाएं। कहीं सहारा नजर नहीं आता। किस्मत ऐसी पलटी कि शाही से फकीरी हो गई। लेकिन फकीरों को चैन और इत्मीनान होता है। यहां वह भी नसीब नहीं।
फौज लड़ती हुई दूर निकल गई थी। बस्ती नदी से पानी लाया। हमने पानी पिया और नवाब नूर महल के चेहरे पर पानी छिड़का। नूर महल रोने लगी और बोलीं कि अभी सपने में तुम्हारे बाबा हज़रत जि़ल्ले सुबहानी को देखा है। जंजीरों में जकड़े हुए हैं और कहते हैं ;
‘‘आज हम गरीबों के लिए यह कांटों भरा खाक का बिछौना मखमली फर्श से बढ़कर है। नूर महल घबराना नहीं। हिम्मत से काम लेना। तकदीर में लिखा था कि बुढ़ापे में ये सख्तियां बर्दाश्त करो। जरा मेरी कुलसूम को दिखा दो। जेलखाने से पहले उसे देखना चाहता हूं।’’
बादशाह की ये बातें सुनकर मेरे मुंह से हाय निकली और आंखें खुल गईं। कुलसूम, क्या सचमुच तुम्हारे बादशाह को जंजीरों में जकड़ा गया होगा ? क्या वाकई वे कैदियों की तरह जेलखाने में भेजे गए होंगे। मिर्जा़ उम्र सुल्तान इसका जवाब दिया कि यह महज वहम है। बादशाह लोग बादशाहों के साथ ऐसा बुरा सुलूक नहीं करते। तुम घबराओ नहीं। वे अच्छे हाल में होंगे। हाफिज मुलतान बादशाह की समधन बोलीं कि ये मुए फिरंगी बादशाहों की कद्र क्या खाक जानेंगे ? वे खुद अपने बादशाह का सिर काटकर सोलह आने में बेचते हैं (सिक्के की तरफ इशारा है जिसमें बादशाह के सिर की पूर्ति होती है—हसन निजा़मी) बुआ, नूर महल, तुमने तो उन्हें जंजीरों में देखा है। मैं कहती हूं कि इन बनिए बक्कालों से तो इससे भी ज्यादा बदसुलूकी दूर नहीं है। लेकिन मेरे शौहर मिर्जा़ ज्यायुद्दीन ने दिलासे की बात करके सबको मुतमयन (शांत) कर दिया।
इतने में बस्ती नाव में गाड़ी को इस पार ले आया और हम सवार होकर चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर शाम हो गई और हमारी गाड़ी एक गाँव में जाकर ठहरी। इस गाँव में मुसलमान राजपूतों की आबादी थी। गांव के नंबरदार ने एक छप्पर हमारे लिए खाली करा लिया जिसमें सूखी घास और फूस का बिछौना था। वे लोग इसी घास पर, जिसको प्याल या पुआल कहते थे, सोते हैं। हमको भी बड़ी खातिरदारी से (जो उनके ख्याल में बड़ी खातिर थी) यह नर्म बिछौना दिया।
मेरा तो इस कूड़े से जी उलझने लगा। पर क्या करते उस वक्त और हो भी क्या सकता था। बेबस होकर इसी में पड़े रहे। दिन भर की तकलीफ और थकान के बाद इत्मीनान और बेफिक्री मिली थी, नींद आ गई।
आधी रात को अचानक हम सब की आंख खुल गई। घास के तिनके सुइयों की तरह बदन में चुभ रहे थे। और पिस्सू जगह-जगह काट रहे थे। उस वक्त की बेचैनी खुदा ही जानता है। मखमली तकियों, रेशमी नर्म-नर्म बिछौनों की आदत थी। इसलिए तकलीफ हुई वरना हम जैसे ही गांव के वे आदमी थे जो गहरी नींद में इसी घास पर पड़े सोते थे। अंधेरी रात में चारों तरफ से सियारों की आवाजें आ रही थीं और मेरा दिल सहमा जाता था। किस्मत को पलटते देर नहीं लगती। कौन कह सकता था कि एक दिन शहनशाहे-हिंद (भारत सम्राट) के बाल-बच्चे यूं खाक पर बसेरे लेते फिरेंगे। इसी तरह कदम-कदम पर तकदीर की गर्दिशों का तमाशा देखते हुए हैदराबाद पहुंचे और सीतारांम पेठ में एक मकान किराए पर ले लिया। जबलपुर में मेरे शौहर ने एक जड़ाऊ अंगूठी जो लूट खसूट से बच गई थी, बेच दी। इसी में रास्ते का खर्च चला और कुछ दिन यहां भी बसर हुए। आखिरकार जो कुछ पल्ले था, खत्म हो गया। अब फिक्र हुई कि पेट भरने का क्या वसीला किया जाए। मेरे शौहर ऊंचे दर्जे के खुशनवीस (लिपिक) थे। उन्होंने दरूद शरीफ ख़त रिहान में लिखा और चार मीनार पर हदिया करने ले गए (उन्होंने बेल बूटे बनाकर बहुत सुंदर ढंग से हजरत मुहम्मद और उनके परिवार के गुण लिखे और चार मीनार पर बेचने ले गए)। लोग उसे देखते थे और हैरानी से उनके मुंह खुले रह जाते थे। पहले दिन दरूद शरीफ की कीमत पांच रुपए पड़ी। इसके बाद यह होने लगा कि जो कुछ वे लिखते फौरन बिक जाता। इस तरह हमारा गुजारा बहुत अच्छी तरह होने लगा। लेकिन मूसा नदी की बाढ़ से डर कर शहर में दरोगा अहमद के मकान में उठ आए। यह आदमी हजूर निजाम का खास मुलाजिम था। इसके बहुत से मकान किराए पर उठे हुए थे।
कुछ दिन बाद खबर उड़ी कि नवाब लशकर जंग, जिसने शहजादों को अपने पास संरक्षण दिया था। अंग्रेजों के कोप में आ गया है और अब कोई आदमी दिल्ली के शहजादों को पनाह नहीं देगा। बल्कि जिस किसी शहजादे की खबर मिलेगी उसके पकड़ने की कोशिश करेगा। हम सब इस खबर से घबरा गए और मैंने अपने शौहर को बाहर निकलने से रोक दिया कि कहीं कोई दुश्मन पकड़वा न दे। घर में बैठे-बैठे फाकों की नौबत आ गई तो लाचार एक नवाब के लड़के को कुरान शरीफ पढ़ाने की नौकरी मेरे शौहर ने बारह रुपये माहवार पर कर ली। वे चुपचाप उनके घर जाते थे और पढ़ा कर लौट आते थे मगर वह नवाब इतने बुरे और कटु स्वभाव के थे कि मेरे शौहर के साथ हमेशा मामूली नौकरों का सा बर्ताव करते थे जिसको वे बर्दाश्त न कर सकते थे और घर आकर रो-रोकर दुआ मांगते थे कि अल्लाह इस जिल्लत की नौकरी से मौत लाख दर्जे बढ़ कर है। तूने इतना मोहताज बना दिया। कभी तो उस नवाब जैसे लोग हमारे गुलाम थे और आज हम उसके गुलाम हैं। इस बीच किसी ने मियां निजा़मुद्दीन साहिब की खबर कर दी। मियां की हैदराबाद में बहुत इज्जत थी क्योंकि मियां हजरत काले मियां साहिब चिश्ती निजा़मी फख़री के साहिबजादे थे जिनको दिल्ली के बादशाह और निजा़म अपनी पीर मानते थे। मियां रात के वक्त हमारे पास आए और हमको देखकर बहुत रोए। एक जमाना था कि जब वे किले में तशरीफ लाते थे तो सोने की कढ़ाई (बेल बूटों) वाली मनसद पर बिठाए जाते थे। बादशाह बेगम अपने हाथ से लौंडियों की तरह सेवा करती थीं। आज वे घर में आए तो टूटा-फूटा बोरिया भी नहीं था जिस पर वे आराम से बैठते। पिछला जमाना आंखों में फिरने लगा। खुदा की जान, क्या था और क्या हो गया। मियां बहुत देर तक हालात पूछते रहे। इसके बाद तशरीफ ले गए। सवेरे उनका पैगाम आया कि हमने खर्च का इंतजाम कर दिया है। अब तुम हज का इरादा कर लो। यह सुनकर दिल खुश हो गया और मक्का मोआजमा की तैयारियां होने लगीं। अलकिस्सा (संक्षेप में) हैदराबाद से रवाना होकर बंबई आए और यहां अपने सच्चे हमदर्द और साथी बस्ती को खर्च देकर वापस भेज दिया। जहाज में सवार होते हुए तो जो मुसाफिर यह सुनता था कि हम हिंदुस्तानी बादशाह के खानदान से हैं तो हमें देखने के लिए उतावला हो उठता था। उस वक्त हम सब दरवेशों के रंग के लिबास में थे। एक हिंदू ने, जिसकी शायद अदन में दुकान थी और जो हमारे हाल से बेखबर था, पूछा कि तुम लोग किस पंथ के फकीर हो। उसके सवाल ने जख्मी दिल पर नमक छिड़क दिया। मैं बोली, ‘‘हम मजलूम (पीड़ित) शाह गुरु के चेले हैं। वही हमारा बाप था वही हमारा गुरु। पापी लोगों ने उसका घरबार सब छीन लिया और हमको उससे जुदा करके जंगलों में निकाल दिया। वे हमारी सूरत को तरसते हैं और हम उनके दर्शन की बगैर बेचैन हैं।
इससे ज्यादा और क्या अपनी फकीरी की हालत बयान करें। जब उसने हमारी असली कैफियत लोगों से सुनी तो बेचारा रोने लगा और बोला कि बहादुर शाह हम सबका बाप और गुरु था। क्या करें, रामजी की यही मर्जी थी कि वह बेगुनाह बरबाद हो।
मक्का पहुंचे तो अल्लाह मियां ने ठहरने का एक अजीब ठिकाना पैदा कर दिया। अब्दुल कादिर नामी मेरा एक गुलाम था जिसको मैंने आजाद करके मक्के भेज दिया था। यहां आकर उसने बहुत दौलत कमाई और ज़मज़म (मक्के में एक जलस्त्रोत, जिसका जल पवित्र माना जाता है) का दरोगा हो गया। उसको हमारे आने की खबर मिली तो दौड़ा हुआ आया और कदमों में गिरकर बहुत रोया। उसका मकान बहुत अच्छा और आरामदेह था। हम सब वहीं ठहरे। कुछ दिनों के बाद सुल्तान रोम के नायब (उप) को जो मक्के में रहता था, हमारी खबर हुई तो वह भी हमसे मिलने आया। किसी ने उससे कहा कि दिल्ली के बादशाह की लड़की आई है। बेहजाबाना (पर्दे के बिना) बातें करती है। नायब सुल्तान ने अब्दुल कादिर के जरिए मुलाकात का पैगाम दिया जो मैंने मंजूर कर लिया।
दूसरे दिन वह हमारे घर आया और बहुत अजब और सलीके से बातचीत की। आखिर में उसने ख्वाहिश की कि वह हमारे आने की खबर हजूर सुल्तान को देना चाहता है। मैंने इसका जवाब बहुत बेपरवाही से दिया कि अब हम एक बहुत बड़े सुल्तान के दरबार में आ गए हैं। अब हमें किसी दूसरे सुल्तान की परवाह नहीं। नायब ने हमारे खर्च के लिए अच्छी खासी रकम मंजूर कर दी और हम नौ वर्ष वहीं रहे। इसके बाद एक साल बगदाद शरीफ वह एक-एक साल नजफ अशरफ व करबला में गुजारा। आखिर इतनी मुद्दत के बाद दिल्ली की याद ने बेचैन किया और वापस दिल्ली आ गए। यहां अंग्रेजों की सरकार ने बहुत तरस खाने के बाद दस रुपये माहवार पेंशन मंजूर कर दी। इस पेंशन की रकम को सुनकर पहले तो मुझे हंसी आई कि मेरे बाप का इतना बड़ा मुल्क लेकर दस रुपए मुआवजा देते हैं। लेकिन फिर ख्याल आया कि मुल्क तो खुदा का है किसी के बाबा की नहीं है, वह जिसको चाहता है दे देता है। जिससे चाहता है, छीन लेता है। इंसान की तो दम मारने की हिम्मत नहीं है।
कुछ साल हुए निधन हो गया। मैंने कई बार शहजादी साहिबा से खुद उनकी जबानी उनके हालात सुने हैं क्योंकि उनको हमारे हुजूर निजा़मुद्दीन औलिया महबूबे अलाही (प्रभु के प्यारे) से खास अकीदत (श्रद्धा) थी। इसलिए अकसर हाजिर होती थीं और मुझे दर्दनाक बातें सुनने का मौका मिलता था। नीचे जितनी भी घटनाएँ दी गई हैं या उनकी साहिबजादी जी़नत ज़मानी बेगम ने, जो अब तक जिंदा हैं और पंडित के कूचे में रहती हैं। ये घटनाएं इस प्रकार हैं।
जिस समय मेरे बाबाजान की बादशाहत खत्म हुई और तख्त-ताज लुटने का वक्त नजदीक आया तो दिल्ली के लालकिला मों कोहराम मचा हुआ था। चारों तरफ हसरत बरसती थी। सफेद-सफेद संगमरमर के मकान काले स्याह नज़र आते थे। तीन वक्त से किसी ने कुछ खाया न था। मेरी गोद में डेढ़ साल की बच्ची जी़नत दूध के लिए बिलखती थी। फिक्र और परेशानी के मारे न मेरे दूध रहा था और न किसी अन्ना के। हम सब इसी उदासी में बैठे थे कि जिल्ले सुबहानी (मुगल दौर में राजा को इसी उपाधि से संबोधित किया जाता था) का खास ख्वाजा सरा हमको बुलाने आया। आधी रात का वक्त, सन्नाटे का आलम, गोलों की गरज से दिल सहम जाते थे, लेकिन हुक्मे सुल्तानी (राजादेश) मिलते ही हम हाजिरी के लिए रवाना हो गए। हुजूर मुसल्ले (नमाज पढ़ने की चटाई) पर तशरीफ रखते थे। तसबीह (जपमाला) हाथ में थी। जब मैं सामने पहुंची और झुककर तीन मुजरे (बंदगी) बजा लाई तो हुजूर ने बहुत प्यार से अपने पास बुलाया और फरमाने लगे, ‘‘कुलसूम, लो अब तुमको खुदा को सौंपा। किस्मत में हुआ तो देख लेंगे। तुम अपने खाविंद (पति) को लेकर फौरन कहीं चली जाओ। मैं भी जाता हूं। जी तो नहीं चाहता कि इस आखिरी वक्त में तुम बच्चों को आंखों से ओझल होने दूं पर क्या करूं साथ रखने में तुम्हारी बरबादी का डर है। अलग रहोगी तो शायद खुदा कोई बेहतरी का सामान पैदा कर दे।’’
इतना फरमाकर हुजूर ने दस्ते मुबारक (कर कमल) दुआ के लिए, जो कंपन रोग के कारण कांप रहे थे, ऊपर उठाए और देर तक ऊंची आवाज में बारगाहे इलाही (अल्लाह का घर) में अर्ज करते रहे :
‘‘खुदा का वंद यह बेवारिस बच्चे तेरे हवाले करता हूं। ये महलों के रहने वाले जंगल वीरानों में जाते हैं। दुनिया में इनका कोई मददगार नहीं रहा। तेमूर के नाम की इज्जत रखियो और इन बेकस औरतों की इज्जत बचाइयो। परवर्दिगार (पालने वाला खुदा) यही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सब हिंदू-मुसलमान मेरी औलाद हैं और आजकल सब पर मुसीबत छाई हुई है। मेरे एमाल (कर्म) की शामत से इनको बेइज्जत न कर और सबको परेशानी से निजात दे।’’
इसके बाद मेरे सिर पर हाथ रखा। जी़नत को प्यार किया और मेरे खाविंद मिर्जा़ ज्यायुद्दीन को कुछ जवाहरात देकर नूर महल साहिबा को हमराह कर दिया। जो हुजूर की बेगम थीं।
पिछली रात को हमारा काफिला किले से निकला। इसमें दो मर्द और तीन औरतें थीं। मर्दों में एक मेरे खाविंद मिर्जा़ ज्यायुद्दीन और दूसरे मिर्जा़ उम्र सुल्तान, बादशाह के बहनोई थे। औरतों में एक मैं, दूसरी नवाब नूर महल और तीसरी हाफिज सुल्तान, बादशाह की समधन थीं। जिस वक्त हम रथ में सवार होने लगे तो तड़के का वक्त था। सब तारे छिप गए थे लेकिन सुबह का तारा झिलमिला रहा था हमने अपने भरे पूरे-घर पर आखिरी नजर डाली तो दिल भर आया और आंसू उमड़ने लगे। नवाब नूर महल की आंखों में आंसू भरे हुए थे और सुबह के तारे का झिलमिलाना नूरमहल की आंखों में नजर आता था।
आखिर लाल से हमेशा के लिए जुदा होकर कोराली गाँव में पहुँचे और वहां अपने रथवान के मकान पर रुके। बाजरे की रोटी और छाछ खाने को मिली। उस वक्त भूख में ये चीजें बिरयानी से भी ज्यादा मजेदार मालूम हुईं। एक दिन तो अमन से गुजर गया। लेकिन दूसरे दिन आस-पास के जाट और गूजर इकट्ठे होकर कोराली को लूटने चढ़ आए। सैकड़ों औरतें भी उनके साथ थीं जो चुड़ैलों की तरह हम लोगों से चिमट गईं। तमाम जेवर और कपड़े इन लोगों ने उतार लिए। जिस वक्त ये सड़ी बसी औरतें अपने मोटे-मोटे, मैले-मैले हाथों से हमारे गले को नोचती थीं तो उनके लहगों से ऐसी बू आती थी कि दम घुटने लगता था।
इस लूट के बाद हमारे पास इतनी भी बाकी न रहा जिससे एक वक्त की रोटी जुट सके। हैरान थे कि देखिए अब और क्या पेश आएगा। जी़नत प्यास के मारे रो रही थी। सामने से एक जमींदार निकला। मैंने बेबस होकर आवाज दी, ‘‘भाई थोड़ा पानी इस बच्ची को ला दे।’’ जमींदार फौरन एक मिट्टी के बरतन में पानी लाया और बोला, ‘‘आज से तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई।’’ यह जमींदार कोराला का खाता-पीता आदमी था। इसका नाम बस्ती था। उसने अपनी बैलगाड़ी तैयार करके हम सब को सवार किया और कहा कि तुम जहां चाहो पहुंचा दूंगा। हमने कहा, ‘‘अजारा, जिला मेरठ में मीर फै़ज अली शाही हकीम रहते हैं। उनसे हमारे खानदान के बहुत अच्छे मरासम (संबंध) हैं। वहां ले चलो।’’ बस्ती हमें अजारा ले गया। मगर मीर फै़ज अली ने ऐसा बुरा बर्ताव किया जिसकी कोई हद नहीं। साफ कानों पर हाथ रख लिए कि तुम लोगों को ठहराकर अपना घरबार तबाह नहीं करना चाहता। (मीर फै़ज अली की औलाद ने यह किताब पढ़ी तो मुझसे कहा कि बेगम साहिबा का बयान ठीक नहीं। मीर फै़ज अली ने उन सबको ठहराया था और मदद दी थी।
वह वक्त बहुत मायूसी का था। एक तो यह डर कि पीछे से अंग्रेज फौज आती होगी। इस पर हमारी हालत इतनी खराब कि हर आदमी की निगाह फिरी हुई थी। वे लोग जो हमारी आंखों के इशारे पर चलते और हर वक्त देखते रहते थे कि हम जो हुक्म दें वह फौरन पूरा किया जाए वही आज हमारी सूरत नहीं देखना चाहते थे। शाबाश है बस्ती जमींदार को कि उसने मुंह बोली बहन का आखिर तक साथ निभाया। बेबस होकर अजारे से रवाना हुए और हैदराबाद की राह पकड़ी। औरतें बस्ती की गाड़ी में सवार थीं और मर्द पैदल चल रहे थे। तीसरे दिन एक नदी के किनारे पहुंचे जहां कोयल के नवाब की फौज डेरा डालकर पड़ी हुई थी। उन्होंने जब सुना कि हम शाही खानदान के आदमी हैं तो बहुत खातिर की और हाथी पर चढ़ाकर नदी के पार उतारा। अभी हम नदी के पार उतरे ही थे कि सामने से फौज आ गई और नवाब की फौज से लड़ाई होने लगी।
मेरे खाविंद मिर्जा़ उम्र सुल्तान ने चाहा कि नवाब की फौज में शामिल होकर लड़ें मगर रिसालदार ने कहला भेजा कि आप औरतों को लेकर जल्दी चले जाएं।
हम जैसा मौका होगा देख लेंगे। सामने खेत थे जिनमें पकी हुई तैयार फसल खड़ी थी। हम लोग उसके अंदर छिप गए। जालिमों ने पता नहीं देख लिया था या अचानक ही गोली लगी। जो कुछ भी एक गोली खेत में आई जिससे आग भड़क उठी औऱ सारा खेत जलने लगा। हम सब वहां से निकलकर भागे पर हाय, कैसी मुसीबत थी—हमको भागना भी नहीं आता था। घास में उलझ-उलझ कर गिरते थे। सिर की चादरें वहीं रह गईं। नंगे सिर होश उड़े हुए हजार दिक्कत से खेत से बाहर आए। मेरे और नवाब महल के पांव लहूलुहान हो गए। प्यास के मारे जबानें बाहर निकल आईं। जी़नत को गश (मूर्छा) पर गश आ रहे थे। मर्द हमको संभालते थे लेकिन हमारा संभलना मुश्किल था।
नवाब नूर महल तो खेत से निकलते ही चकरा कर गिर पड़ीं और बेहोश हो गईं। मैं जी़नत को छाती से लगाए अपने खाविंद का मुंह देख रही थी और दिल में कहती थी कि अल्लाह हम कहां जाएं। कहीं सहारा नजर नहीं आता। किस्मत ऐसी पलटी कि शाही से फकीरी हो गई। लेकिन फकीरों को चैन और इत्मीनान होता है। यहां वह भी नसीब नहीं।
फौज लड़ती हुई दूर निकल गई थी। बस्ती नदी से पानी लाया। हमने पानी पिया और नवाब नूर महल के चेहरे पर पानी छिड़का। नूर महल रोने लगी और बोलीं कि अभी सपने में तुम्हारे बाबा हज़रत जि़ल्ले सुबहानी को देखा है। जंजीरों में जकड़े हुए हैं और कहते हैं ;
‘‘आज हम गरीबों के लिए यह कांटों भरा खाक का बिछौना मखमली फर्श से बढ़कर है। नूर महल घबराना नहीं। हिम्मत से काम लेना। तकदीर में लिखा था कि बुढ़ापे में ये सख्तियां बर्दाश्त करो। जरा मेरी कुलसूम को दिखा दो। जेलखाने से पहले उसे देखना चाहता हूं।’’
बादशाह की ये बातें सुनकर मेरे मुंह से हाय निकली और आंखें खुल गईं। कुलसूम, क्या सचमुच तुम्हारे बादशाह को जंजीरों में जकड़ा गया होगा ? क्या वाकई वे कैदियों की तरह जेलखाने में भेजे गए होंगे। मिर्जा़ उम्र सुल्तान इसका जवाब दिया कि यह महज वहम है। बादशाह लोग बादशाहों के साथ ऐसा बुरा सुलूक नहीं करते। तुम घबराओ नहीं। वे अच्छे हाल में होंगे। हाफिज मुलतान बादशाह की समधन बोलीं कि ये मुए फिरंगी बादशाहों की कद्र क्या खाक जानेंगे ? वे खुद अपने बादशाह का सिर काटकर सोलह आने में बेचते हैं (सिक्के की तरफ इशारा है जिसमें बादशाह के सिर की पूर्ति होती है—हसन निजा़मी) बुआ, नूर महल, तुमने तो उन्हें जंजीरों में देखा है। मैं कहती हूं कि इन बनिए बक्कालों से तो इससे भी ज्यादा बदसुलूकी दूर नहीं है। लेकिन मेरे शौहर मिर्जा़ ज्यायुद्दीन ने दिलासे की बात करके सबको मुतमयन (शांत) कर दिया।
इतने में बस्ती नाव में गाड़ी को इस पार ले आया और हम सवार होकर चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर शाम हो गई और हमारी गाड़ी एक गाँव में जाकर ठहरी। इस गाँव में मुसलमान राजपूतों की आबादी थी। गांव के नंबरदार ने एक छप्पर हमारे लिए खाली करा लिया जिसमें सूखी घास और फूस का बिछौना था। वे लोग इसी घास पर, जिसको प्याल या पुआल कहते थे, सोते हैं। हमको भी बड़ी खातिरदारी से (जो उनके ख्याल में बड़ी खातिर थी) यह नर्म बिछौना दिया।
मेरा तो इस कूड़े से जी उलझने लगा। पर क्या करते उस वक्त और हो भी क्या सकता था। बेबस होकर इसी में पड़े रहे। दिन भर की तकलीफ और थकान के बाद इत्मीनान और बेफिक्री मिली थी, नींद आ गई।
आधी रात को अचानक हम सब की आंख खुल गई। घास के तिनके सुइयों की तरह बदन में चुभ रहे थे। और पिस्सू जगह-जगह काट रहे थे। उस वक्त की बेचैनी खुदा ही जानता है। मखमली तकियों, रेशमी नर्म-नर्म बिछौनों की आदत थी। इसलिए तकलीफ हुई वरना हम जैसे ही गांव के वे आदमी थे जो गहरी नींद में इसी घास पर पड़े सोते थे। अंधेरी रात में चारों तरफ से सियारों की आवाजें आ रही थीं और मेरा दिल सहमा जाता था। किस्मत को पलटते देर नहीं लगती। कौन कह सकता था कि एक दिन शहनशाहे-हिंद (भारत सम्राट) के बाल-बच्चे यूं खाक पर बसेरे लेते फिरेंगे। इसी तरह कदम-कदम पर तकदीर की गर्दिशों का तमाशा देखते हुए हैदराबाद पहुंचे और सीतारांम पेठ में एक मकान किराए पर ले लिया। जबलपुर में मेरे शौहर ने एक जड़ाऊ अंगूठी जो लूट खसूट से बच गई थी, बेच दी। इसी में रास्ते का खर्च चला और कुछ दिन यहां भी बसर हुए। आखिरकार जो कुछ पल्ले था, खत्म हो गया। अब फिक्र हुई कि पेट भरने का क्या वसीला किया जाए। मेरे शौहर ऊंचे दर्जे के खुशनवीस (लिपिक) थे। उन्होंने दरूद शरीफ ख़त रिहान में लिखा और चार मीनार पर हदिया करने ले गए (उन्होंने बेल बूटे बनाकर बहुत सुंदर ढंग से हजरत मुहम्मद और उनके परिवार के गुण लिखे और चार मीनार पर बेचने ले गए)। लोग उसे देखते थे और हैरानी से उनके मुंह खुले रह जाते थे। पहले दिन दरूद शरीफ की कीमत पांच रुपए पड़ी। इसके बाद यह होने लगा कि जो कुछ वे लिखते फौरन बिक जाता। इस तरह हमारा गुजारा बहुत अच्छी तरह होने लगा। लेकिन मूसा नदी की बाढ़ से डर कर शहर में दरोगा अहमद के मकान में उठ आए। यह आदमी हजूर निजाम का खास मुलाजिम था। इसके बहुत से मकान किराए पर उठे हुए थे।
कुछ दिन बाद खबर उड़ी कि नवाब लशकर जंग, जिसने शहजादों को अपने पास संरक्षण दिया था। अंग्रेजों के कोप में आ गया है और अब कोई आदमी दिल्ली के शहजादों को पनाह नहीं देगा। बल्कि जिस किसी शहजादे की खबर मिलेगी उसके पकड़ने की कोशिश करेगा। हम सब इस खबर से घबरा गए और मैंने अपने शौहर को बाहर निकलने से रोक दिया कि कहीं कोई दुश्मन पकड़वा न दे। घर में बैठे-बैठे फाकों की नौबत आ गई तो लाचार एक नवाब के लड़के को कुरान शरीफ पढ़ाने की नौकरी मेरे शौहर ने बारह रुपये माहवार पर कर ली। वे चुपचाप उनके घर जाते थे और पढ़ा कर लौट आते थे मगर वह नवाब इतने बुरे और कटु स्वभाव के थे कि मेरे शौहर के साथ हमेशा मामूली नौकरों का सा बर्ताव करते थे जिसको वे बर्दाश्त न कर सकते थे और घर आकर रो-रोकर दुआ मांगते थे कि अल्लाह इस जिल्लत की नौकरी से मौत लाख दर्जे बढ़ कर है। तूने इतना मोहताज बना दिया। कभी तो उस नवाब जैसे लोग हमारे गुलाम थे और आज हम उसके गुलाम हैं। इस बीच किसी ने मियां निजा़मुद्दीन साहिब की खबर कर दी। मियां की हैदराबाद में बहुत इज्जत थी क्योंकि मियां हजरत काले मियां साहिब चिश्ती निजा़मी फख़री के साहिबजादे थे जिनको दिल्ली के बादशाह और निजा़म अपनी पीर मानते थे। मियां रात के वक्त हमारे पास आए और हमको देखकर बहुत रोए। एक जमाना था कि जब वे किले में तशरीफ लाते थे तो सोने की कढ़ाई (बेल बूटों) वाली मनसद पर बिठाए जाते थे। बादशाह बेगम अपने हाथ से लौंडियों की तरह सेवा करती थीं। आज वे घर में आए तो टूटा-फूटा बोरिया भी नहीं था जिस पर वे आराम से बैठते। पिछला जमाना आंखों में फिरने लगा। खुदा की जान, क्या था और क्या हो गया। मियां बहुत देर तक हालात पूछते रहे। इसके बाद तशरीफ ले गए। सवेरे उनका पैगाम आया कि हमने खर्च का इंतजाम कर दिया है। अब तुम हज का इरादा कर लो। यह सुनकर दिल खुश हो गया और मक्का मोआजमा की तैयारियां होने लगीं। अलकिस्सा (संक्षेप में) हैदराबाद से रवाना होकर बंबई आए और यहां अपने सच्चे हमदर्द और साथी बस्ती को खर्च देकर वापस भेज दिया। जहाज में सवार होते हुए तो जो मुसाफिर यह सुनता था कि हम हिंदुस्तानी बादशाह के खानदान से हैं तो हमें देखने के लिए उतावला हो उठता था। उस वक्त हम सब दरवेशों के रंग के लिबास में थे। एक हिंदू ने, जिसकी शायद अदन में दुकान थी और जो हमारे हाल से बेखबर था, पूछा कि तुम लोग किस पंथ के फकीर हो। उसके सवाल ने जख्मी दिल पर नमक छिड़क दिया। मैं बोली, ‘‘हम मजलूम (पीड़ित) शाह गुरु के चेले हैं। वही हमारा बाप था वही हमारा गुरु। पापी लोगों ने उसका घरबार सब छीन लिया और हमको उससे जुदा करके जंगलों में निकाल दिया। वे हमारी सूरत को तरसते हैं और हम उनके दर्शन की बगैर बेचैन हैं।
इससे ज्यादा और क्या अपनी फकीरी की हालत बयान करें। जब उसने हमारी असली कैफियत लोगों से सुनी तो बेचारा रोने लगा और बोला कि बहादुर शाह हम सबका बाप और गुरु था। क्या करें, रामजी की यही मर्जी थी कि वह बेगुनाह बरबाद हो।
मक्का पहुंचे तो अल्लाह मियां ने ठहरने का एक अजीब ठिकाना पैदा कर दिया। अब्दुल कादिर नामी मेरा एक गुलाम था जिसको मैंने आजाद करके मक्के भेज दिया था। यहां आकर उसने बहुत दौलत कमाई और ज़मज़म (मक्के में एक जलस्त्रोत, जिसका जल पवित्र माना जाता है) का दरोगा हो गया। उसको हमारे आने की खबर मिली तो दौड़ा हुआ आया और कदमों में गिरकर बहुत रोया। उसका मकान बहुत अच्छा और आरामदेह था। हम सब वहीं ठहरे। कुछ दिनों के बाद सुल्तान रोम के नायब (उप) को जो मक्के में रहता था, हमारी खबर हुई तो वह भी हमसे मिलने आया। किसी ने उससे कहा कि दिल्ली के बादशाह की लड़की आई है। बेहजाबाना (पर्दे के बिना) बातें करती है। नायब सुल्तान ने अब्दुल कादिर के जरिए मुलाकात का पैगाम दिया जो मैंने मंजूर कर लिया।
दूसरे दिन वह हमारे घर आया और बहुत अजब और सलीके से बातचीत की। आखिर में उसने ख्वाहिश की कि वह हमारे आने की खबर हजूर सुल्तान को देना चाहता है। मैंने इसका जवाब बहुत बेपरवाही से दिया कि अब हम एक बहुत बड़े सुल्तान के दरबार में आ गए हैं। अब हमें किसी दूसरे सुल्तान की परवाह नहीं। नायब ने हमारे खर्च के लिए अच्छी खासी रकम मंजूर कर दी और हम नौ वर्ष वहीं रहे। इसके बाद एक साल बगदाद शरीफ वह एक-एक साल नजफ अशरफ व करबला में गुजारा। आखिर इतनी मुद्दत के बाद दिल्ली की याद ने बेचैन किया और वापस दिल्ली आ गए। यहां अंग्रेजों की सरकार ने बहुत तरस खाने के बाद दस रुपये माहवार पेंशन मंजूर कर दी। इस पेंशन की रकम को सुनकर पहले तो मुझे हंसी आई कि मेरे बाप का इतना बड़ा मुल्क लेकर दस रुपए मुआवजा देते हैं। लेकिन फिर ख्याल आया कि मुल्क तो खुदा का है किसी के बाबा की नहीं है, वह जिसको चाहता है दे देता है। जिससे चाहता है, छीन लेता है। इंसान की तो दम मारने की हिम्मत नहीं है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book